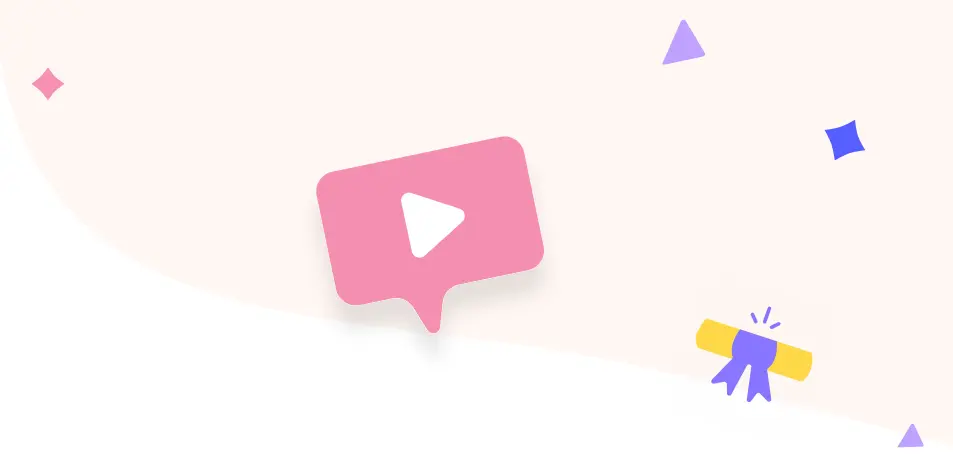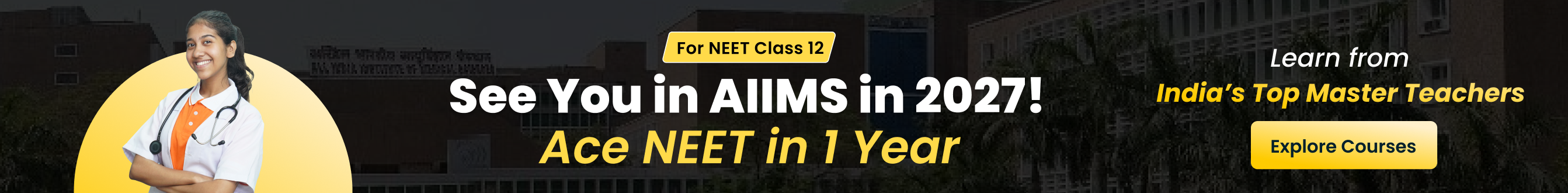Solved NCERT Questions For Class 12 Chemistry Chapter 9 In Hindi - Free PDF
FAQs on NCERT Solutions For Class 12 Chemistry In Hindi Chapter 9 Coordination Compounds - 2025-26
1. Where can I find reliable and step-by-step NCERT Solutions for Class 12 Chemistry Chapter 9, Coordination Compounds?
You can find comprehensive and accurate NCERT Solutions for Class 12 Chemistry Chapter 9, Coordination Compounds, on the Vedantu website. These solutions are prepared by subject matter experts and are aligned with the latest CBSE 2025-26 syllabus, providing detailed, step-by-step answers to all textbook questions.
2. What topics are covered in the NCERT Solutions for Class 12 Chemistry Chapter 9?
The NCERT Solutions for Chapter 9, Coordination Compounds, cover all the exercises from the textbook. The topics include:
- Werner's theory of coordination compounds.
- Definitions of key terms like ligand, coordination number, and coordination sphere.
- IUPAC nomenclature for writing names and formulas.
- Isomerism in coordination compounds (structural and stereoisomerism).
- Bonding theories, including Valence Bond Theory (VBT) and Crystal Field Theory (CFT).
- Applications of coordination compounds in various fields.
3. Are solutions for both in-text and end-of-chapter exercises included for Coordination Compounds?
Yes, the NCERT Solutions for Class 12 Chemistry Chapter 9 provide complete and detailed answers for both the in-text questions and the end-of-chapter exercises. This ensures a thorough understanding of all concepts as you progress through the chapter.
4. How do the NCERT solutions explain the correct method for writing IUPAC names of coordination compounds?
The NCERT solutions provide a systematic, step-by-step method for solving IUPAC nomenclature questions. The process involves:
- Identifying the cation and anion in the coordination compound.
- Naming the ligands alphabetically, followed by the central metal atom.
- Calculating the oxidation state of the central metal atom and writing it in Roman numerals.
- Using appropriate suffixes like '-ate' for anionic complexes.
5. What is the step-by-step approach used in the NCERT solutions to explain isomerism in coordination compounds with examples?
The solutions explain isomerism by first categorising it into structural isomerism (like linkage, coordination, ionisation, and solvate) and stereoisomerism (geometrical and optical). For each type, the solutions:
- Provide a clear definition.
- Use specific examples from the NCERT textbook, such as [Co(NH₃)₅(NO₂)]Cl₂.
- Illustrate the structures of different isomers (e.g., cis-trans and d-l pairs) to show the spatial arrangement of ligands.
6. How do the NCERT solutions use Valence Bond Theory (VBT) to explain the geometry and magnetic properties of complexes like [Fe(CN)₆]⁴⁻?
The solutions break down the VBT application into clear steps:
- Determine the oxidation state of the central metal ion (e.g., Fe²⁺).
- Write its electronic configuration.
- Identify the type of ligand (strong-field like CN⁻ or weak-field).
- Show the hybridisation of metal orbitals (e.g., d²sp³ for inner orbital or sp³d² for outer orbital complexes).
- Fill the hybrid orbitals with electron pairs from ligands.
- Determine the geometry (e.g., octahedral) and predict magnetic properties (paramagnetic or diamagnetic) based on unpaired electrons.
7. How do the solutions for Chapter 9 illustrate the concept of d-orbital splitting in Crystal Field Theory (CFT)?
The NCERT solutions illustrate d-orbital splitting with clear energy level diagrams. They explain that in an octahedral field, the five degenerate d-orbitals split into two sets: the lower-energy t₂g set (dxy, dyz, dzx) and the higher-energy e₉ set (dx²-y², dz²). The energy difference between these sets is defined as the Crystal Field Splitting Energy (Δ₀), which is crucial for explaining the colour and magnetic properties of complexes.
8. Why is it important to follow the step-by-step method given in the NCERT solutions for determining the oxidation state and coordination number?
Following the step-by-step method is crucial because these two values are fundamental to understanding a coordination compound. The oxidation state is essential for correctly naming the complex using IUPAC rules and for applying bonding theories like VBT and CFT. The coordination number directly determines the geometry of the complex (e.g., 4 for tetrahedral/square planar, 6 for octahedral), which is key to understanding its isomerism and reactivity. A mistake in these initial steps can lead to incorrect conclusions about the entire structure.
9. The NCERT solutions differentiate between double salts and complex compounds (like in Q2). What is the fundamental difference in their ionisation that students often miss?
The fundamental difference lies in their identity in an aqueous solution. A double salt, like Mohr's salt (FeSO₄·(NH₄)₂SO₄·6H₂O), completely dissociates into its constituent ions (Fe²⁺, NH₄⁺, SO₄²⁻). In contrast, a complex compound, like K₄[Fe(CN)₆], dissociates to give a complex ion, [Fe(CN)₆]⁴⁻, which does not break down further into Fe²⁺ and CN⁻ ions. The NCERT solutions clarify that the entities inside the square brackets (the coordination sphere) remain intact in solution.
10. According to the NCERT solutions, how does the nature of a ligand (strong-field vs. weak-field) affect the magnetic properties and electronic configuration of a complex?
The NCERT solutions explain this using Crystal Field Theory. A strong-field ligand (like CN⁻, CO) causes a large crystal field splitting (high Δ₀). This forces electrons to pair up in the lower energy t₂g orbitals before filling the e₉ orbitals, resulting in low-spin complexes that are often diamagnetic or have fewer unpaired electrons. Conversely, a weak-field ligand (like H₂O, Cl⁻) causes a small splitting (low Δ₀), allowing electrons to occupy the higher energy e₉ orbitals before pairing up, leading to high-spin complexes with more unpaired electrons and stronger paramagnetic behaviour.
11. While solving NCERT questions on isomerism, what is a common mistake students make when trying to distinguish between geometrical and optical isomers for octahedral complexes?
A common mistake is failing to check for a plane of symmetry. Students might correctly identify a 'cis' isomer but incorrectly assume it is always optically active. For example, in an [MA₄B₂] type complex, the cis-isomer is optically active, but the trans-isomer is optically inactive due to the presence of a plane of symmetry. The NCERT solutions guide students to draw the structures and visualise their mirror images to determine if they are non-superimposable, which is the true test for optical activity.
12. How do the NCERT solutions explain the practical applications of coordination compounds as mentioned in the textbook exercises?
The solutions highlight several key applications based on textbook questions. They explain the role of coordination compounds in:
- Biological systems: For example, haemoglobin (an iron complex) as an oxygen carrier and chlorophyll (a magnesium complex) in photosynthesis.
- Metallurgy: Used in the extraction of metals like gold and silver through the formation of cyanide complexes, such as [Au(CN)₂]⁻.
- Analytical chemistry: Used for the detection and estimation of metal ions, like the use of DMG for Ni²⁺ detection.
- Medicine: For instance, the use of cis-platin, a platinum complex, in cancer therapy.