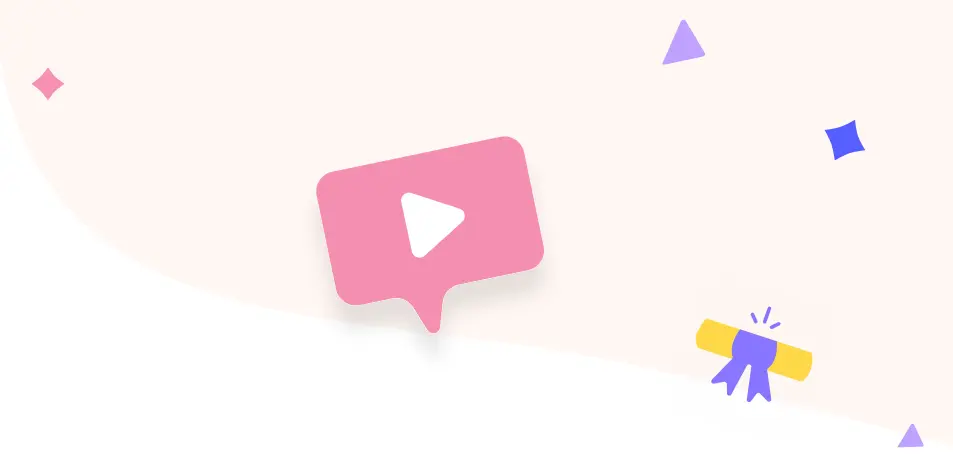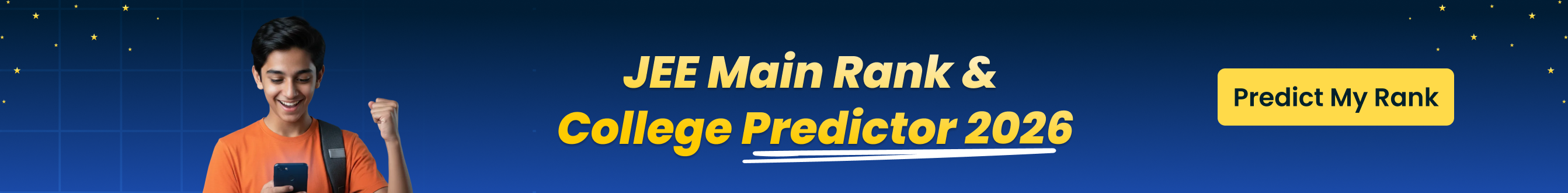Step-by-Step Solutions For Class 12 Biology Chapter 13 In Hindi - Free PDF Download
FAQs on NCERT Solutions For Class 12 Biology in Hindi Chapter 13 Organisms and Populations (2025-26)
1. How should I use Vedantu's NCERT Solutions for Class 12 Biology Chapter 13 to effectively prepare for the board exams?
To best utilise these solutions, you should first attempt to solve the NCERT textbook questions for 'Organisms and Populations' on your own. Afterwards, use our solutions to compare and verify your answers. Pay close attention to the step-by-step methodology, the inclusion of specific keywords, and the answer structure, all of which are designed as per the latest CBSE 2025-26 pattern to help you secure maximum marks.
2. What is the correct method for solving numerical problems on population growth rate as per the NCERT exercises?
When solving for population growth rate, it's crucial to first identify the growth model required. For exponential growth, use the formula dN/dt = rN. For logistic growth, the correct formula is dN/dt = rN((K-N)/K). Our NCERT solutions provide a clear, step-by-step breakdown for each numerical problem, showing how to correctly substitute values for births, deaths, carrying capacity (K), and intrinsic rate of increase (r).
3. How can I accurately draw and label age pyramid diagrams for expanding and stable populations as required in NCERT questions?
For a complete answer, follow this method:
- Expanding Population: Draw a pyramid with a very broad base, representing a high percentage of pre-reproductive individuals, and a narrow top for post-reproductive individuals.
- Stable Population: Draw a structure that is more bell-shaped, where the number of pre-reproductive and reproductive individuals is almost equal.
Always label the Y-axis with the three age groups (Pre-reproductive, Reproductive, Post-reproductive) and the X-axis with the population size or percentage.
4. When solving an NCERT question about population interactions, how do I correctly distinguish between parasitism and predation in my answer?
While both are (+/-) interactions, the key distinction in your answer should be the mechanism and outcome. For predation, state that the predator kills and consumes the prey instantly. For parasitism, explain that the parasite typically lives in or on the host, deriving nourishment over a longer period without immediately killing it. The host's fitness is reduced. Using specific examples provided in our NCERT solutions, like a tiger and deer for predation versus a human liver fluke for parasitism, will strengthen your answer.
5. Why is the logistic growth model considered a more accurate method for solving most NCERT problems than the exponential model?
The logistic growth model is more realistic and often the required method because it incorporates the concept of carrying capacity (K). This reflects that resources in any habitat are finite and cannot support unlimited population growth. While the exponential model shows hypothetical growth with unlimited resources, the logistic model provides a solution that accounts for environmental resistance, a key ecological principle emphasized in the CBSE curriculum.
6. The latest NCERT syllabus for 2025-26 lists 'Organisms and Populations' as Chapter 11, not 13. How are these solutions relevant?
You are correct; the NCERT syllabus has been rationalised, and 'Organisms and Populations' is now Chapter 11 in new textbooks. These solutions are maintained under Chapter 13 to assist students using older, widely circulated editions. Rest assured, the question-and-answer content is fully aligned with the topics and exercises prescribed in the current CBSE 2025-26 syllabus for this chapter, ensuring complete and accurate exam preparation.
7. How should I structure an answer explaining an organism's adaptations, for instance, a kangaroo rat, as per the CBSE pattern?
A well-structured answer should identify the type of adaptation and then explain its mechanism. For a kangaroo rat, you should mention:
- It exhibits physiological adaptations to its desert habitat.
- It conserves water by excreting highly concentrated urine.
- It meets its water requirements through internal fat oxidation, where water is a by-product, a fact often highlighted in NCERT exercises.
This approach of classifying and then explaining is the standard method for scoring full marks.
8. In the Verhulst-Pearl Logistic Growth equation, what does the term ‘(K-N)/K’ actually represent and why is it essential to mention in an answer?
The term (K-N)/K in the logistic growth equation represents environmental resistance. It is the factor that slows population growth as it approaches the carrying capacity (K). Explaining this concept in your answer is crucial as it demonstrates a deeper understanding beyond simple formula application. It shows you recognize that as a population (N) grows, the pressure from limited resources increases, which in turn reduces the per capita rate of increase.